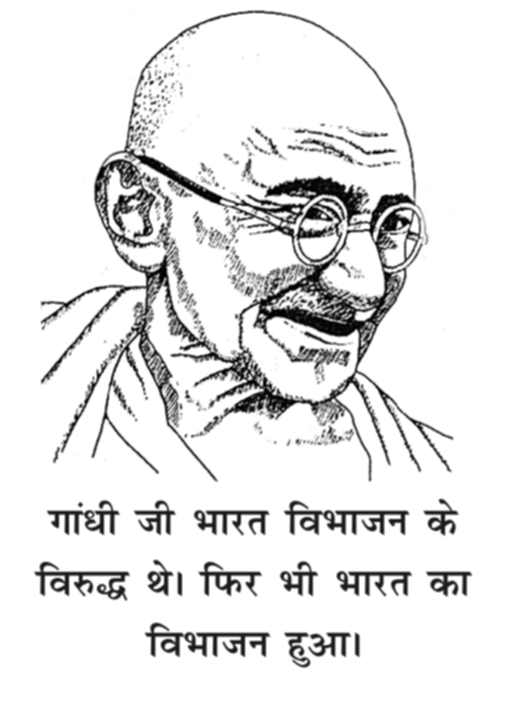लेख चितरंजन लाल भारती
जाह्नवी फरवरी 2023 गणतंत्र विशेषांक
अंग्रेजों की ‘बांटों और राज करो’ की राजनीति में कैसे कैसे दाँव-पेंच चले गए तथा तत्कालीन नेताओं द्वारा उनका विरोध किस प्रकार किया गया, प्रस्तुत है एक
विश्लेषण।
अंग्रेजों की लगभग दो सौ साल की गुलामी के बाद भारतवर्ष 1947 ई- में स्वतंत्र हुआ। मगर अखण्ड रूप में नहीं, बल्कि टुकड़ों के रूप में। किन्तु जिस सांप्रदायिकता के सवाल को हल करने के लिए भारत का विभाजन हुआ था, वह अपनी जगह ज्यों-त्यों रह गया। उसी समय से यह सवाल भी उठने लगा कि क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही? चूंकि स्वतंत्रता-संग्राम के सेनापति के रूप में महात्मा गांधी की भूमिका निर्विवाद रही है, उनकी तरफ इशारा होते रहना स्वाभाविक था।
अब तक के साक्ष्यों के मिले आधार पर आइने की तरह यह बात साफ हो जाती है कि गांधी जी भारत विभाजन के विरुद्ध थे। फिर भी भारत का विभाजन हुआ, इसमें उनकी क्या भूमिका रही अथवा उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं। इन्हें जाने बगैर हम किसी निष्पक्ष फैसले तक पहुंच ही नहीं सकते।
1857 ई- के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम, जिसे ‘सिपाही विद्रोह’ के नाम से भी जाना जाता है, के बाद भारतीयों को खासकर मुसलमानों को अंग्रेज शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। वह इस कारण कि प्रथम बार मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। इस संघर्ष के भारतीय नेता के रूप में, वह चाहे दिखावे के रूप में ही क्यों न हो, मुसलमान बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जबकि वास्तविक अर्थो में उस वक्त तक मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली और इसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गया था।
1885 ई- में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ जो गांधी के आगमन तक अभिजात एवं कुलीन वर्गों की पार्टी मानी जाती थी। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत में अनेक पुनर्जागरण आंदोलन हुए, जिससे हिन्दुओं में पर्याप्त धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक आंदोलन हुए। इससे हिन्दुओं में धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक बदलाव हुए ही, उनमें अपने प्राचीन सभ्यता-संस्कृति एवं धर्म के प्रति गौरव का भान भी हुआ।
मगर मुसलमान इससे विमुख से रहे। हालांकि मुसलमानों में भी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक बदलाव के लिए आंदोलन हुआ था, जो ‘अलीगढ़ आंदोलन’ के नाम से भी जाना जाता है। इसका श्रेय प्रमुखतः सर सैयद अहमद को दिया जाता है। उन्होंने यूं तो भारतीय मुस्लिम जगत् को कई रचनात्मक आंदोलन दिये, मगर स्वतंत्रता-संग्राम के मामले में उनकी स्थिति विभाजक सी रही। वे अंग्रेज भक्त के रूप में ही प्रस्तुत रहे। यह उस समय की उनकी विवशता भी थी। आखिर ‘आधुनिक भारत के पितामह’ माने जाने वाले राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों के समर्थन पर ही तो सतीप्रथा, स्त्री-शिक्षा, बाल-विवाह निषेध आदि आंदोलनों का सफलतापूर्वक संचालन किया था।
अंग्रेज मुसलमानों को संदेह की
दृष्टि से देखते थे
सर सैयद अहमद 1887 ई- के बाद ही कांग्रेस का विरोध करने लगे थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि अंग्रेज चूंकि मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखते थे और इसलिए उनका समर्थन कांग्रेस को मिलता था, जबकि सर सैयद अहमद अपनी, खासकर मुसलमानों की, नजदीकियां अंग्रेजों के साथ बढ़ाना चाहते थे। वे हिन्दुओं की मानसिकता से भय खाते और घृणा भी करते थे।
वह प्रजातंत्र या लोकतंत्र को संदेह की दृष्टि से देखते थे, जो कि कांग्रेस का आदर्श और लक्ष्य भी था। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर भारत स्वतन्त्र हुआ तो बहुमत रखने वाले हिन्दुओं का भारत में शासन होगा और इससे अल्पमत वाले मुस्लिमों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना था कि यदि भारत में लोकतंत्र हुआ, तो यहां दो ही दल हिन्दुओं और मुसलमानों के होंगे। वह लोकतंत्र का आधार समानता, जनसंख्या आदि को न मानकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अधिप्रतिनिधित्व आरक्षण और ऐतिहासिक महत्त्व के आधार पर शासन की मांग करते थे। उनका मानना था कि मुसलमान एक अलग कौम है, जो कभी भारत में शासन करती थी। इस तरह उन्होंने 1886 ई- से ही भारत में विवादास्पद मुस्लिम राजनीति के चरणों की शुरूआत कर दी। यहां ध्यातव्य यह भी है कि अब अंग्रेज परोक्ष रूप से उन्हें समर्थन देने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी कांग्रेस से भय होने लगा था।
हिन्दी-उर्दू का जबर्दस्त विवाद
1898 ई- में सर सैयद अहमद के निधन के उपरांत भी मुस्लिम नेताओं का यही प्रयास रहा कि मुसलमानों को कांग्रेस से अलग-थलग रखा जाए। इस बीच कांग्रेस ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाये कि अंग्रेज कांग्रेस के प्रति और सशंकित हो उठे। वह समझ गये कि जब तक मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग कर लड़ाया नहीं गया उनका भारत में शासन करना कठिन होगा।
उन्हीं दिनों हिन्दी-उर्दू का जबर्दस्त विवाद भी उठा। उर्दू प्रांतीय अदालतों की भाषा थी। उस वक्त तक उर्दू के साथ हिन्दी को भी लिये जाने की मांग उठी। 1900 ई- में संयुक्त प्रांत (उ-प्र-) के गवर्नर ने उर्दू के साथ हिन्दी को भी अदालतों की भाषा बना दिया। इससे मुस्लिमों में काफी रोष हुआ। उन्हें लगा कि अंग्रेज हिन्दुओं के साथ मिलकर उनकी अस्मिता पर चोट कर रहे हैं। 1904 ई- में अलीगढ़ में मुस्लिमों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि भारत एक कौम नहीं, बल्कि कई कौमों का एक महाद्वीप है।
ऐतिहासिक तथ्यों को यदि आधार मानें तो यह सिद्धांत गलत सिद्ध होता है। भारत में हिन्दू और मुसलमानों के अलावा बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई आदि मतावलंबी भी हैं और मूलतः यहीं के निवासी हैं। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही उनका विभिन्न धर्मों में धर्मांतरण हुआ है। इसलिए मुसलमान भी मूलतः यहीं के निवासी हैं। यह भी सही है कि कट्टर मुस्लिम शासकों के अत्याचार से बचने के लिए भी लोगों ने धर्म-परिवर्तन किया था। इस तरह भारत एक कौम हुआ। मगर अंग्रेज शासकों और कट्टरवादियों ने इस तर्क और सिद्धांत को मान्यता नहीं दी, क्योंकि उन्हें तो इसी आधार पर भारतीय समाज को टुकड़ों में बांटना था और फूट की आग पर अपनी रोटी सेंकनी थी।
दूसरी तरफ विभिन्न संगठनों, खासकर कांग्रेस के माध्यम से, हिन्दू समुदाय में अनेक समाज-सुधार के कार्य होते रहे। कांग्रेस में सभी मतों और मान्यताओं को मानने वाले तपे-तपाए नेता थे। उनमें से कुछ एक तरफ अंग्रेज शासकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर हिन्दू धर्म की खामियों को दूर करने और उसका गौरव गान करने में भी लगे थे। मगर मुसलमानों के बीच ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। वह बस अपने अतीत की शासकीय श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। ‘अलीगढ़ आंदोलन’ बिखर गया था और वह भी सिर्फ उ-प्र- (संयुक्त प्रांत) तक सीमित था।
मुस्लिम लीग की स्थापना
मुस्लिम सिर्फ बंगाल और पंजाब प्रांत में बहुमत में थे। उन्हें लगता था कि हिन्दू कांग्रेस की आड़ लेकर बहुमत की राजनीति कर रहे हैं। अंततः 1906 ई- में ढाका में ‘मुस्लिम लीग’ की स्थापना की गई। उन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के संबंध में यह नहीं सोचा कि उनमें भी अनेक धार्मिक, सामाजिक अंतर्विरोध हैं और उनका द्वंद्व अब सामने आ रहा है और उन लोगों के लिए भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष के साथ-साथ धार्मिक-सामाजिक कट्टरताओं और कुरीतियों से भी लड़ना उनकी मजबूरी बन गई है। जो भी हो, सर सैयद अहमद ने मुस्लिम राजनीति का जो बीजारोपण किया था, अब वह पुष्पित-पल्लवित होकर वृक्ष का आकार ग्रहण करने लगा था और जिसे बाद में जिन्ना जैसे नेेताओं ने खाद-पानी देकर अपनी राजनीति चलाने के लिए खूब इस्तेमाल किया। हालांकि वह एक राष्ट्रवादी नेता थे, मगर परिस्थिति और उनकी महत्त्वाकांक्षाओं ने उन्हें सांप्रदायिक नेता बना दिया।
अंग्रेजों ने मुस्लिमों को
फुुसलाना और संरक्षण देना शुरू कर दिया
वर्ष 1905 ई- में अंग्रेजों द्वारा किये गये सांप्रदायिक ‘बंगाल के विभाजन’ के विरुद्ध भारत में एक स्वतः स्फूर्त स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उस वक्त कांग्रेस में भी जबर्दस्त अंतर्विरोध थे, जो 1907 ई- में ‘सूरत कांग्रेस’ के अधिवेशन में देखने को मिले। बढ़ते हुए तीव्र आंदोलनों को देखकर अंततः अंग्रेजों ने 1911 ई- में बंगभंग योजना को रद्द कर दिया। मगर इसके साथ ही वह भारत की राजधानी को कलकत्ता से उठाकर दिल्ली ले आए तथा बंगाल को अलग कर दो नए राज्य बिहार और उड़ीसा बना दिये। इस बीच अंग्रेजों ने मुस्लिमों को फुुसलाना और संरक्षण देना शुरू कर दिया। वे लोग भी उनके पीछे इस कारण खुशी-खुशी हो लिये कि उन लोगों की जो मांगें और संकल्पनाएं थीं, वे अंग्रेजों की सहमति के बगैर संभव नहीं थी।
1909 ई- में
‘मोर्ले-मिंटो योजना’
1909 ई- में लार्ड मोर्ले ने गवर्नर जनरल मिंटो को एक सुधार योजना प्रस्तुत करने को कहा, जो इतिहास में ‘मोर्ले-मिंटो योजना’ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें यूं तो अनेक बातें हैं, मगर इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात ये थी कि केन्द्रीय एवं प्रांतीय कौंसिलों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणालियां बनाई गई थीं। मुसलमानों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाये गए थे, जहां सिर्फ मुसलमान ही उम्मीदवार हो सकते थे। फिर निर्वाचनों के लिए वोट देने के लिए हिन्दू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं। आगे चलकर यही विष-वृक्ष भारत में सांप्रदायिकता के उभार और विभाजन का कारण बना।
उस वक्त तक गांधीजी भारत में कहीं थे ही नहीं, जो उन्हें इसके लिए दोषी करार दिया जाय। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1914 ई- में लौटे थे। वह आने के साथ ही भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान नहीं करने लगे, बल्कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत को सही अर्थों में समझने-पहचानने के लिए देश भर का दौरा करने लगे। इस बीच उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में निलहे जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध सफल आंदोलन कर विश्वसनीयता भी हासिल कर ली थी।
कांग्रेस तो शुरू से ही अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध थी। अब मुस्लिम लीग ने भी समझ लिया था कि अंग्रेजों को सिर्फ अपने स्वार्थ और सत्ता से मतलब है और वह इसके लिए उनका सिर्फ इस्तेमाल भर कर रहे हैं। वह समझ गए थे कि बिना आंदोलन किये अथवा दबाव डाले अंग्रेज किसी को कुछ नहीं देने वाले। 1916 ई- में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। दोनों ने ही अलग-अलग एक योजना स्वीकार की, जिसे ‘कांग्रेस लीग स्कीम’ अथवा ‘लखनऊ समझौता’ कहा जाता है।
लखनऊ समझौता तक गांधी की कांग्रेस में कोई विशेष महत्ता नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस में बाल-पाल-लाल अर्थात् बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का डंका बजता था। लखनऊ समझौता देखने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उस वक्त कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। उसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा उनके अधिप्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। इस समझौते से तात्कालिक फायदा चाहे जो हुआ हो, इसके दूरगामी प्रभाव अत्यंत भयंकर हुए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन मानकर एक तरह से स्वयं को केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में मान लिया और अपने को राष्ट्रीय दल कहलाने के दावे को सदैव के लिए दुर्बल कर दिया। हालांकि लखनऊ समझौते को बंगाल और पंजाब के मुस्लिम नेताओं द्वारा स्वीकृति नहीं मिली। कारण कि इस समझौते से उनके व्यापक स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती थी। एक कारण यह भी था कि उधर मुस्लिम लीग का प्रभाव अत्यन्त कम था।
पूरे देश में सांप्रदायिकता का
जहर फैल चुका था
1920 ई- में जब गांधी सक्रिय राजनीति में उतरे, तब तक पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल चुका था। गांधी को ब्रिटिश सत्ता और सांप्रदायिकता के अलावा सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों से भी लंबी लड़ाई लड़नी थी। वह सभी बातों को अपनी पैनी निगाहों से देख-परख रहे थे। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने पराजित तुर्की का विभाजन कर दिया तो दुनिया भर के मुसलमानों ने इसके विरोध में ‘खिलाफत आंदोलन’ चलाया, क्योंकि वे तुर्की के सुलतान को मुस्लिम जगत् का खलीफा मानते थे। भारत में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं अली बंधुआें के नेतृत्व में ‘खिलाफत आंदोलन’ चल रहा था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन इसलिए किया कि वह उन्हें सत्य और न्याय पर आधारित दिखाई दिया।
नवंबर 1919 ई- में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन, दिल्ली ने गांधीजी को अपना अध्यक्ष चुन लिया। गांधी जी द्वारा इसे समर्थन देने का एक अन्य कारण यह भी था कि अगर हिन्दुओं द्वारा मुस्लिमों की न्यायोचित मांगों का समर्थन किया गया तो यह हिन्दू-मुस्लिम-एकता तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सहायक होता। गांधी ने 1 अगस्त 1920 ई- में खिलाफत के सवाल पर असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। इसे कांग्रेस ने सिंतबर 1920 ई- में एक विशेष अधिवेशन में तथा दिसंबर के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी कर दिया।
असहयोग आंदोलन
ब्रिटिश-सत्ता को हिला दिया
5 फरवरी 1922 ई- तक असहयोग आंदोलन की आग देश के कोने-कोने तक फैल गई थी। गांधी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में माने जाने लगे। पहली बार करोड़ों भारतीयों ने, जिनमें निम्न तबके के किसान-मजदूर से लेकर छोटे-बड़े जमींदार और राजे-रजवाड़े भी शामिल थे, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कमर कसकर लड़ाई लड़ी। यह आंदोलन जन-जन के मन में पैठ कर गया था। हिन्दू-मुसलमानों ने कमर कसकर समान रूप से संघर्ष कर ब्रिटिश-सत्ता को सही अर्थों में हिला दिया। मगर गोरखपुर स्थित चौरी-चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। दरअसल गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलनकारी थक रहे हैं और उनमें निराशा फैल रही है जिससे आंदोलन हिंसक हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसे स्थगित कर दिया।
जिन्ना जब ‘मुस्लिम लीग’ को
बकवास मानते थे
खिलाफत आंदोलन से उत्पन्न सांप्रदायिक सद्भाव कुछ मुस्लिम नेताओं को ‘संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र’ के पक्ष में प्रभावित कर रहा था। उसमें जिन्ना प्रमुख थे। यह वहीं जिन्ना थे, जो ‘मुस्लिम लीग’ को बकवास और बाल गंगाधर तिलक को हमेशा राष्ट्रीय नेताओं में सर्वोपरि मानते थे। तिलक के मुकदमों की पैरवी उन्होंने जमकर की थी। पुनः अपने ‘इंडिपेंडेंट दल’ के साथ 1924 ई- में मोतीलाल नेहरू के साथ सहयोग किया था। चूंकि वह सम्मिलित निर्वाचन के पक्ष में थे, इसलिए दूसरे मुस्लिम नेताओं खासकर बंगाल-पंजाब के मुस्लिम नेताओं ने उन्हें सदैव हाशिये पर रखने की कोशिश की।
फरवरी 1925 ई- में ‘साइमन कमीशन’ आया और अपना प्रस्ताव रखा। इसमें अन्य बातों के अलावा प्रमुखतः यह था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और अधिप्रतिनिधित्व के नियमों को लागू रहना चाहिए। उसने यह भी चुनौती पेश की कि वह कोई ऐसा प्रारूप बनाकर दिखा दे, जिससे सभी राजनीतिक दल सहमत हों। निःसंदेह यह एक कठिन चुनौती थी। कांग्रेस ने फरवरी 1928 ई- में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया। राजनीतिक दलों में तीखे मतभेद तो थे ही। फिर भी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया।
1928 ई- के ‘नेहरू रिपोर्ट’ की आलोचना अली बंधुओं ने
आरंभ कर दी
दिसंबर 1928 ई- में इस ‘नेहरू रिपोर्ट’ पर एक सर्वदलीय सम्मेलन में विचार किया गया। यूं तो इस रिपोर्ट में कई विशेषताएं थीं, मगर उसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह था कि निर्वाचन प्रणाली को वयस्क मताधिकार और क्षेत्रीय निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। हालांकि अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित थे, इस रिपोर्ट की आलोचना अली बंधुओं ने आरंभ कर दी। वे इस सम्मेलन से ही उठकर चले गए और विभिन्न प्रांतों में घूम-घूमकर सांप्रदायिकता का प्रचार करने लगे। मो- शफी और जिन्ना के अलग-अलग मुस्लिम लीगी दल थे, जिनमें जिन्ना का मुस्लिम लीग सर्वाधिक कमजोर था। या यूं कहें कि इसे विभिन्न मुस्लिम राजनीतिक दलों द्वारा कमजोर कर दिया गया था, क्योंकि जिन्ना ‘संयुक्त निर्वाचन प्रणाली’ के पक्ष में थे। मो- शफी ने आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया और मांग की कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और अधिप्रतिनिधित्व बना रहे। जिन्ना ने अपनी राजनीतिक स्थिति ठीक करने के लिए एक दस-सूत्री मांग पेश की, जिसमें सभी मुस्लिम वर्गों की मांगें थीं। मगर फिर भी जब उनका नेतृत्व दुर्बल ही रहा तो वह अत्यंत निराश होकर इंग्लैण्ड चले गए। ध्यातव्य यह है कि नेहरू रिपोर्ट को अन्य दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अस्वीकृत कर दिया था।
गोलमेज सम्मेलन मुस्लिम दलों
के कड़े प्रतिरोध
1930 ई- में ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के हिस्सा न लेने के कारण वह असफल रहा। पुनः 1931 ई- में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को अधिकृत किया गया। हालांकि वह एक अन्य प्रतिनिधि बिहार के आंदोलनकारी अब्दुल कÕयूम अंसारी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर मुस्लिम दलों के कड़े प्रतिरोध के कारण वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सके। अभी तक तो बात सांप्रदायिक प्रणाली और अधिप्रतिनिधित्व को बहाल रखने अथवा खत्म करने की चल रही थी, किन्तु गोलमेज सम्मेलनों में दूसरे संगठनों, खासकर दलित वर्ग, के लिए अलग आरक्षण और निर्वाचन प्रणाली की बात उठ आई। सम्मेलन में सभी लोग अपने-अपने दलों के हितों की बात कर रहे थे। एक अकेले गांधी वहां अखण्ड भारत का सपना देख रहे थे। अंततः उन्हें वहां से खाली हाथ निराश होकर लौटना ही था। हालांकि इसके बाद एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ, मगर उसका विशेष महत्त्व न था।
गोलमेज सम्मेलनों के असफल होने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डोनल्ड ने 1932 ई- में कम्यूनल एवार्ड (सांप्रदायिक निर्णय) की घोषणा कर दी। उसने पृथक् निर्वाचन पद्धति पर बल दिया था। पहले जहां भारतीयों को दस (10) टुकड़े में बांटा जाना था, वहीं अब उनके अठारह (18) टुकड़े बना दिये गये थे, जिनमें दलित वर्ग प्रमुख था। कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। मगर गांधी इसके विरुद्ध दृढ़ संकल्प लिये हुए थे। वह हिंदुओं से दलितों को किसी भी मूल्य पर कटने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में ही यह घोषणा कर दी थी कि यदि किसी ने हिन्दुआें से दलितों को अलग करने की कोशिश की तो वह जान की बाजी लगा देंगे।
सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध पहले तो गांधी ने ब्रिटिश शासकों के साथ पत्रचार किया। उनसे संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वह 20 दिसंबर 1932 ई- से अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठने से ब्रिटिश शासकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, सो नहीं पड़ा। परन्तु अन्य हिन्दू नेताओं पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा।
मदन मोहन मालवीय एवं अन्य उन जैसे प्रमुख हिन्दू नेताओं ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर से गंभीर विचार-विमर्श आरंभ कर एक समझौते पर आए और इस प्रकार उस समझौते के फलस्वरूप गांधी जी का अनशन 26 दिसंबर 1932 ई- को टूटा। उस समय की परिस्थितियों में गांधी ऐसा न करते, तो अंग्रेजों की भारत को छिन्न-भिन्न करने की चाल सफल हो जाती और तब पाकिस्तान जैसे दलितिस्तान, सिखिस्तान और जाने क्या-क्या टुकड़े बन जाते। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की यही तो विशेषता थी। बाद में गांधी जी की मौजूदगी में अंबेडकर एवं मदन मोहन मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के साथ हुआ समझौता ‘पूना पैक्ट’ के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते के अनुसार 148 स्थान दलितों के लिए आरक्षित किये गये। हरिजनों तथा हिन्दुओं के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे मान्यता दे दी गई।
हिन्दुओं के बहुमत बनाने
की राजनीति
गांधी जी के इस कार्य से मुस्लिमों को लगा कि इस तरह अब वह हिन्दुओं के बहुमत बनाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि वह सिर्फ भारतीय समाज के ज्यादा टुकड़े न हों, इसी प्रयास में लगे थे। जो भी हो, तभी से खासकर जिन्ना का मत परिवर्तन होने लगा और वह मुस्लिम कट्टरवादिता की तरफ झुकने लगे थे। ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा—’ लिखने वाले प्रसिद्ध शायर इकबाल तो ‘पूना पैक्ट’ के मुखर विरोधी थे। उन्होंने 1930 ई- में प्रथमतः कल्पित ‘पाकिस्तान’ की अवधारणा रखी, जिसे जिन्ना ने उस वक्त ‘बकवास’ कहकर टाल दिया था। किन्तु आगे चल कर वही जिन्ना इसके सूत्रधार बने। उधर गांधी को सांप्रदायिकता के साथ अनेक मोर्चो पर लड़ाई लड़नी थी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से लेकर देशी रजवाड़ों और जमींदारी, जमीन-बंदोबस्त, राष्ट्रीय शिक्षा, नारी शिक्षा, शराबबंदी, किसानों और मजदूरों की समस्याएं एक तरफ थीं, तो दूसरी तरफ हरिजनोद्धार, ग्रामोद्धार, पंचायती राज, स्वावलम्बन, स्वास्थ्य-सफाई एवं स्वदेशी का महत्त्व आदि। अनगिनत बातें थीं, जिनके प्रति जनता को जागरूक करना था। एक तरफ क्रूर और सख्त ब्रिटिश सरकार थी तो दूसरी तरफ अनगिनत नेताओं की महत्त्वकांक्षाएं थीं, जिन्हें नियंत्रित करना भी एक समस्या थी।
1935 ई- के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 ई- में प्रांतीय सभा के चुनाव हुए। कांग्रेस ने चमत्कारी प्रदर्शन करते हुए कुल 1538 स्थानों में से 711 स्थान प्राप्त किये। छः प्रांतों में इसका बहुमत रहा। मगर पंजाब, बंगाल और सिंध में इसकी स्थिति शोचनीय रही। पंजाब में इसको 86 में से केवल 2 और बंगाल में 119 में से केवल 40 स्थान मिले। हालांकि संपूर्ण भारत की दृष्टि से मुस्लिम लीग को भी असफल ही कहा जा सकता है। उसको अपने अल्पसंख्यक प्रांतों में ही सफलता मिली थी। जो भी हो, यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि 50 वर्षों की सक्रिय राजनीति करने के बावजूद मुस्लिमों में कांग्रेस लोकप्रिय नहीं हो सकी थी और उसकी छवि ‘हिन्दू पार्टी’ बन कर रह गई थी अथवा बना दी गई थी।
जिन्ना मुस्लिमों के नेता
बन गए
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में मो- इकबाल ने 1930 ई- में पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिमों के लिए जिस एक राज्य ‘पाकिस्तान’ की कल्पना की थी, वही पाकिस्तान की मांग के लिए औचित्य बना। जिन्ना का इंग्लैण्ड से पुनरागमन हो चुका था और वह नए सिरे से मुस्लिम लीग का पुनर्गठन करने में लगे थे। नतीजतन 1937 ई के निर्वाचन में लीग की सफलता उल्लेखनीय रही। बंगाल, पंजाब और सिंध के भी प्रांतीय मुस्लिम दल चाहते थे कि अखिल भारतीय स्तर पर उनकी बात कांग्रेस के समकक्ष रखनेवाली कोई राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। सो पहले जिन्ना को जमीन और अब छत मिल गई थी। जिन्ना अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिमों के नेता बन गए। अब वह ‘ंसंयुक्त निर्वाचन प्रणाली’ के बदले ‘सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली’ के मुखर प्रवक्ता बन गए थे। अब वह और उनका दल मुस्लिम लीग विभिन्न प्रांतीय सभाओं के कांग्रेसी नेताओं और मंत्रिमंडल के बारे में झूठी-सच्ची अफवाहें और घृणा फैलाने में लग गये थे। मुस्लिम लीग का बस अब इतना ही अभिप्राय था कि उसे मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि दल मान लिया जाए।
गांधी जहां भारतीय समस्याओं का हल दो पक्षों-कांग्रेस और ब्रिटिश सत्ता के द्वारा संभव मानते थे, वहीं जिन्ना यह मानते थे कि समस्या का समाधान चार पक्षों के मध्य हो सकता है। दो अन्य पक्ष थेµमुस्लिम लीग और भारतीय रजवाड़े। 1938 ई- के बाद तो जिन्ना कांग्रेस को राष्ट्रीय दल की अपेक्षा हिन्दू दल खुलेआम कहने लगे थे।
मुस्लिम लीग के वार्षिक
अधिवेशन में ‘पाकिस्तान प्रस्ताव’ पास कर दिया गया
23 मार्च 1940 ई- को मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध ‘पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव’ पास कर दिया गया। हालांकि प्रस्ताव अस्पष्ट था। फिर जिन्ना ने इस प्रस्ताव की व्याख्या करने से स्पष्ट इंकार भी कर दिया। इससे यह महसूस होता है कि यह सौदेबाजी का एक ढंग भर था। फिर भी ध्यातव्य है कि 1940-46 ई- के बीच जितने संवैधानिक प्रस्ताव रखे गए, उन्हें मुस्लिम लीग ने तब तक स्वीकार नहीं किया, जब तक कि केन्द्रीय प्रस्ताव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग समानता, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और केन्द्र के नियंत्रण से मुक्ति नहीं मिल गई। कांग्रेस के लिए यह सब असंभव कार्य थे। कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों से बाहर अथवा विरुद्ध कैसे जाती और अपना राष्ट्रीय स्वरूप क्योंकर खोती। और इस मामले में अकेले गांधी भी अलग-थलग पड़ रहे थे। वह कांग्रेस को अपने दिखाये रास्ते से हटने को कह भी नहीं सकते थे। साथ ही उनका मुस्लिम लीग को समझाने-बुझाने का सारा प्रयास निष्फल सिद्ध हो रहा था। ऐसे में भारत का विभाजन साफ दिख रहा था। 8 अगस्त 1942 ई- को ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन व्यापक रूप से शुरू हुआ। उस वक्त तक कांग्रेस के अनेक नेता सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की मांग को अनचाहे ही सही स्वीकार करने लगे थे। जुलाई 1944 ई- में राजगोपालचारी ने देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए एक फार्मूला प्रकाशित किया, जो इतिहास में उन्हीं के नाम पर ‘राजगोपालचारी फार्मूला’ के नाम से प्रसिद्ध है तथा भारत का विभाजन भी उसी आधार पर हुआ।
‘राजगोपालचारी फार्मूला’ के आधार पर गांधी और जिन्ना के बीच दो सप्ताह तक वार्त्ता चली। मगर असफल रही। कारण कि गांधी भारतीय विभाजन को ‘वयस्क मताधिकार’ के आधार पर देखना चाहते थे, जबकि जिन्ना चाहते थे कि यह विभाजन बिना जनमत के हो। वह तो एक कदम आगे मुस्लिम बहुल राज्यों में जनमत ही नहीं चाहते थे। पुनः इसे जिन्ना स्वतंत्रता पूर्व चाहते थे, जबकि गांधी जी बाद में। सो इसे असफल तो होना ही था। जिन्ना ने अपने स्वभाव के अनुरूप अडि़यल रुख अपना लिया था। इस वार्त्ता के बाद जिन्ना और अधिक महत्त्वपूर्ण बन गए थे, क्योंकि गांधी जी ने उनसे लंबी वार्त्ता की थी। विभाजन की बात देशभर में अब सबकी जुबान पर चढ़ने लगी थी।
गांधी की भारत विभाजन
में क्या भूमिका रही
1945 ई- में केन्द्रीय विधान सभा और प्रांतीय सभा के लिये चुनाव हुए। सामान्य स्थानों पर कांग्रेस को तथा आरक्षित स्थानों पर मुस्लिम लीग को भारी सफलता मिली। इन चुनावों से अब यह बात साफ हो गई कि कांग्रेस का मुसलमानों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वास्तव में मुस्लिम लीग ही करती है। इस कटु यथार्थ को नेहरू-पटेल जैसे कांग्रेसी नेता ही नहीं, बल्कि गांधी भी समझने लगे थे। वह सक्रिय राजनीति से अलग होने की सोचने लगे। अलग भी हो गए। फिर भी गांधी ने अंत-अंत तक जिन्ना को समझाने का असफल प्रयास किया, यहां तक कि उन्हें अखण्ड भारत का प्रधानमंत्री तक स्वीकार करते हुए उन्हें बने रहने की गारंटी भी देनी चाही।
गांधी की भारत विभाजन में क्या भूमिका रही, यह सवाल ही बेतुका है। वह तो शुरू से अंत तक इसके विरुद्ध थे। वह जीवन भर सांप्रदायिकता से संघर्ष करते रहे और अंत में सांप्रदायिकता के भूत ने ही उनके जीवन का अंत भी कर दिया। उन्हें हिन्दू अथवा मुसलमान बताने के बजाय सच्चा मनुष्य बताना ज्यादा सही है। भारत का विभाजन 20वीं सदी का एक कटु यथार्थ है, जो साम्राज्यवादियों की राजनीतिक देन थी। ‘सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली’ असंवैधानिक ही नहीं, अमानवीय और असामाजिक कृत्य था, जो मक्कारी भर तरीके से भारत पर थोप दिया गया था। डॉ- राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार ‘भारत का विभाजन जिन्ना या किसी अन्य द्वारा नहीं हुआ, बल्कि वह लार्ड मिंटो के कारण हुआ, जिसने 1909 ई- में पृथक् निर्वाचन प्रणाली दी थी।’