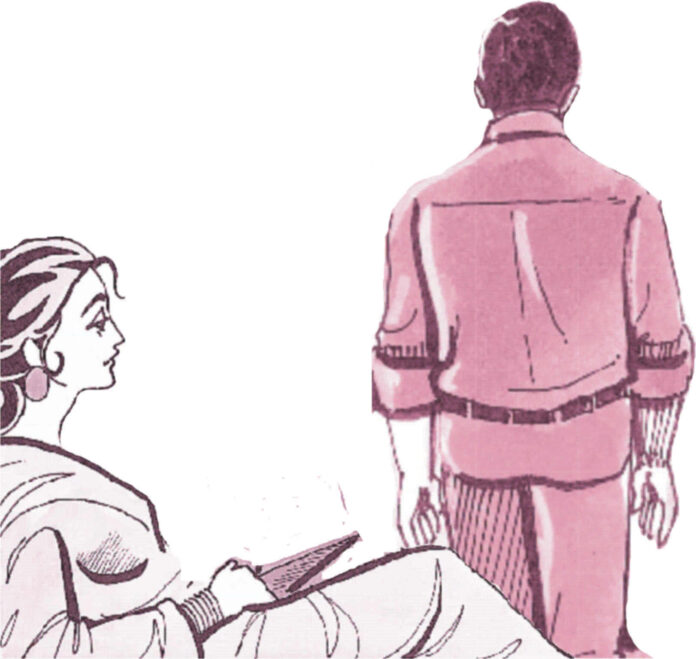कहानी
डॉ. अशोक रस्तोगी
युवा हृदय कवियाें में विशेष रूप से विपरीत लिंगों में
घनिष्ठ काव्य मैत्री हो जाती है जिससे उनके गृहस्थ जीवन में
अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही एक परस्पर समर्पित
काव्य मैत्री की दुखद कहानी।
जुलाई, 2023
स्वास्थ्य विशेषांक
पीले पोस्टकार्ड पर लिखे लड़खड़ाते से गिने-चुने शब्दों पर मेरी दृष्टि स्थिर होकर रह गई।
स्नेहिल अपर्णा!
जीवन की इस अंतिम संध्या में यदि एक बार आकर मुझसे मिल सको तो शांति के साथ कभी न टूटने वाली गहरी नींद में सो सकूंगा। और तुम्हारा उपकार मानूंगा। प्रार्थना बस यही है कि विलंब मत करना। कहीं ऐसा न हो जाए कि पिंजरे का पंछी तुम्हारे आने से पूर्व ही नीलांबर की अनंत यात्र पर निकल जाए।
-प्रोफेसर सत्यकाम विद्यालंकार, परमार्थ निकेतन,
ट्टषिकेश।
करुणा और तड़पन से भरी इस याचना ने तन-मन को उद्वेलित तो किया ही साथ ही कर्तव्यजनित भावना को भी उकसा दिया। अटैची में दो साडि़यां, एक डायरी तथा कुछ अन्य सामान रखकर तैयार हुई ही थी कि पतिदेव सामने अड़ कर खड़े हो गए-‘रानी साहिबा इस तरह बिना बताए अचानक सज-धजकर आज कहां जा रही हैं? यह तो बच्चों की परीक्षाओं का भी वक्त नहीं है। अतः प्रैक्टिकल लेने जाने का भी बहाना नहीं बनाया जा सकता। अकारण क्याें समय और पैसा बरबाद करती रहती हो?
शक्की पति के इस विष जैसे कटाक्ष पर मैं झुंझला उठी, ‘कभी तो समय की संवेदनशीलता को समझ लिया करो जी! क्यों हर समय यह नुकीले तंज कसते रहते हो, नौकरी करनी है और समाज में प्रतिष्ठा पानी है तो बाहर तो आना जाना पड़ेगा ही। खैर आज तो मैं कालेज के कार्य से नहीं अपितु साहित्यिक संगोष्ठी में भाग लेने हरिद्वार जा रही हूं। बड़े-बड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकारों का जमावड़ा है। ऐसी संगोष्ठी में भाग लेने का दुर्लभ अवसर बड़े सौभाग्य से मिल पाता है। परसों रात्रि तक लौट आऊंगी।’ मैंने सरासर झूठ बोल दिया——–सत्य बोलती तो असंख्य प्रश्न उछल गए होते सत्यकाम तुम्हारा क्या लगता है? क्या प्रयोजन है उससे? मर रहा है तो मरने दो, दुनिया मर रही है। सबकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का ठेका तुम्हीं ने ले रखा है क्या? कब से संबंध है उससे? आदि-आदि।
जयपुर से आगरा तक का उबाऊ सफर—-मन तो करता था कि बस को पंख लग जाएं और मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। पर बस को रामायण के पुष्पक विमान की तरह मेरे मन के अनुसार थोड़े ही चलना था वह तो मदमाती, इठलाती, कदम-कदम पर विश्राम लेती अपनी ही धीर मंथर गति से चल रही थी।
आगरा से ट्टषिकेश वाली सीधी टेªन में चढ़ी तो बड़ी भीड़ थी। साथ-साथ धक्का-मुक्की भी। प्रतीत होता था सभी यात्रियों को आज ही ट्टषिकेश अथवा हरिद्वार जाना है। बड़ी मुश्किल से भीतर घुस पाई। भीतर तो बहुत ही बुरा हाल था। कोई मुंह में बीड़ी सिगरेट सुलगाए धुंए के छल्ले उड़ा रहा था तो कोई चार-पांच यात्रियों की सीट पर अकेला पसरा मुंह में गुटखा चबा रहा था और कहीं भी झट से थूक देता था। कहीं किसी सीट पर कई-कई यात्री गुथ कर बैठे थे। और खाली जगहों पर उनके गट्ठर व पोटलियां फैली पड़ी थीं। स्वयं पर ही झुंझलाहट होने लगी—क्यों अकारण बैठे-बिठाए यह मुसीबत मोल ले ली? सत्यकाम जी से मिलना क्या इतना जरूरी था? 25 वर्षों से उनसे जब कोई संवाद नहीं हो पाया तब क्या इस संवादहीनता को कुछ दिनों के लिए और नहीं टाला जा सकता था?
अलीगढ़ तक एक टांग पर खडे़ होकर आना पड़ा। कहीं लेशमात्र भी तो जगह नहीं बन पा रही थी जहां अपने नितंब टिका सकती। वह कोई भला मानस ही था कोई जिसने ऊपर की बर्थ पर लेटे-लेटे ही आंखें मसलते हुए मुझसे पूछा-‘मैम कौन सा स्टेशन आ गया?’
‘अलीगढ़ !’ मेरे इतना कहते ही वह झट से नीचे कूद पड़ा और मेरी अटैची को ऊपर रखते हुए उदारतापूर्वक बोला-‘आप आगरे से खड़ी-खड़ी आ रही हैं कुछ देर आराम कर लीजिए! वैसे आप जाएंगी कहां तक?’ ‘हरिद्वार’ मेरे मुंह से निकलना था कि भाई खीसें निपोरने लगा-‘समझ गया किसी पाप का प्रायश्चित करने जा रही होंगी? गंगा में डुबकी लगाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। दुनिया पहुंचती है जी वहां अपने पापों को धोने। जाना तो मुझे भी हरिद्वार पर अलीगढ़ का कोई काम ध्यान आ गया, अब उसे निपटाकर ही आगे बढ़ूंगा। हो सकता है आपकी मेरी अगली भेंट गंगा तट पर हरिद्वार में ही हो जाए।’
ऊपर की बर्थ अधिकार में आते ही मुझे ऐसे संतोष की अनुभूति हुई जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई हो। चादर बिछाकर ब्रीफकेस सिर के नीचे लगाकर लेटी तो आंखें स्वतः ही मूंदने लगीं। और अशांत मन विपत्र स्मृतियों की अंधी सुरंग से गुजरता हुआ 25 वर्ष पुराने अतीत में जा पहुंचा। जब संस्कृत के प्रोफेसर लब्धप्रतिष्ठ सुनामधन्य साहित्यकार सत्यकाम विद्यालंकार जी को पहली बार देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था।
‘हमारे’ महाविद्यालय में त्रिदिवसीय सांस्कृतिक आयोजन ‘कोलाहल’ का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करने मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे थे सत्यकाम विद्यालंकार जी। साहित्यप्रेमियों के लिए जाना पहचाना नाम था विद्यालंकार जी का। साहित्य के क्षेत्र में आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे थे वे। पत्र-पत्रिकाएं उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती थी। संपादक और प्रकाशक उनसे पत्र व्यवहार करने अथवा साक्षात्कार करने को अधीर हुए रहते थे। इसीलिए महाविद्यालय में उनके आगमन की सूचना मात्र से नगर भर में कोलाहल सा मच गया। साहित्य पिपासुओं का तो मानो कोई पूर्व कल्पित दिवास्वप्न पूर्ण होने जा रहा था। सभी महाविद्यालय की ओर ऐसे दौड़ पड़े जैसे मधुमक्खियों के नासारन्ध्रो में कहीं से मधु की भीनी गंध घुस गई हो।
गोरा चिट्टा रंग रूप, भूरे घुंघराले केश, तेजोदीप्त आंखें, अद्भुत देहयष्टि और विलक्षण व्यक्तित्व———-सर्वाधिक प्रभावित हुई थी मैं उनकी सरलता और सादगी पर। मोहविष्ट सी निर्निमेष उन्हें बस निहारती रह गई। और सोचती रह गई कि यह खादी के दुग्ध धवल परिधान में लिपटा सीधा सादा सा आदमी किस प्रकार ऐसी भावप्रवण कविताएं और मर्मस्पशी कहानियां लिख पाता होगा? उनके मुख से निकला एक-एक शब्द मेरे हृदय में ऐसी अमिट छाप छोड़ रहा था जैसे उनका स्वर किसी दिव्यलोक से आ रहा हो। अंत में उन्होंने नवोदित कथाकारों और कवियों को संदेश भी दिया था। नवोदित साहित्यकारों को चाहिए कि अपनी रचनाओं में आम आदमी की पीड़ा को उकेरें। विपन्नता के दर्शन कराएं। अभावाें की झलक दिखाएं। कभी मेरी आवश्यकता अनुभव करें तो बेझिझक संपर्क करें। नवोदित रचनाकारों के लिए मेरे घर का दरवाजा सदैव खुला रहता है। धन्यवाद।
उनकी यह उदारता तो मेरे दिल को छू ही गई थी। कविताएं मैं भी लिखती थी। बहुत सारी कविताएं लिख डाली थीं। किंतु दुर्भाग्यवश कहीं किसी पत्रिका में 4 पंक्तियां भी प्रकाशित नहीं हो सकी थी। हर कविता पर मैं बहुत मेहनत करती, बार-बार शब्दों को तोड़ती-मरोड़ती, संशोधन करती और अंतिम रूप देकर उत्साह से लबालब पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी पत्रिका को भेज देती। संपादक के नाम अनुरोध पत्र भी लिखती। किंतु कुछ ही दिनों बाद सारा उत्साह क्षीण पड़ जाता जब कविता संपादक के खेद सहित वापस लौट आती। अपनी बेबसी पर मैं रो ही पड़ती।
तब क्या मेरे दुर्भाग्य का अंत होने जा रहा है? क्या विधाता ने ही ऐसे उदार गुरु के दुर्लभ संयोग का अद्भुत अवसर प्रदान किया है मुझे? मैं सोचने लगी थी कि विद्यालंकार जी को अपनी कविताएं दिखाकर संशोधन का अनुरोध करूंगी। फिर देखूं कैसे नहीं छपेंगी मेरी कविताएं?
पर सौभाग्य का यह अवसर भी हाथ से निकल गया। विद्यालंकार जी मंच से उतरे ही थे कि प्रशसकों की भीड़ ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे आज के बाद वे फिर कभी हाथ नहीं आएंगे—जैसे वे चुंबक हो और प्रशंसक लोहकण—विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न—आपकी पहली रचना कौन सी थी? साहित्य सफर कहां से शुरू हुआ था? इतनी उत्कृष्ट रचनाएं कैसे लिख लेते हैं? प्रेरणास्त्रेत कौन है? अन्य साहित्यकारों की तरह पत्नी ही या कोई और? आपका यह सफर कहां जाकर पूर्ण होगा? सर्वाधिक चर्चित रचना किसे मानते हैं?
प्रशंसकों की भीड़ छंटी भी नहीं थी कि पत्रकार आ चिपटे और आयोजक गण उन्हें अतिथि कक्ष में ले गए।
सौभाग्य तरु का फल हाथ आते-आते रह गया था। निराश सी, अन्यमनस्क सी घर लौटी तो किसी भी काम में मन नहीं लगा। चेतना विद्यालंकार जी के चारों ओर दौड़ती रही। उनका अद्भुत सौंदर्यमयी सरल व्यक्तित्व हृदय में इतनी गहराई तक पैठ कर गया था कि किसी भी पल उस आभामंडल की चकाचौंध से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाती थी। शीतल उद्विग्नता रक्त के बिन्दु-बिन्दु में समाहित हो गई थी।
और कुछ नहीं सूझा तो मैंने उन्हें डरते-डरते एक पत्र लिख दिया-‘सुविस्तृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र को मेरा प्रणाम। संचित साहित्य वारिधि में से चुल्लू भर किसी को दे देने से कोई कमी नहीं आ जाती। मेरी अकिंचन लेखनी के यदि आपकी कलम सजा संवारकर स्थापित कर सके तो आजन्म ट्टणी रहूंगी। विनम्र अनुरोध है कि संलग्न कविता को परिमार्जित रूप प्रदान कर आशीष वर्षण के साथ तत्काल प्रेषित करें-प्रतीक्षारत -अपर्णा दत्ता, मुरादाबाद।
पत्र को पत्रलय में डालते हुए मन के किसी कोने में भय मिश्रित शंका के कृमि भी कुलबुला रहे थे कि इतने बड़े साहित्यकार को इस प्रकार पत्र लिखना क्या ठीक रहा? कहीं किसी शब्द से रुष्ट हो गए तो? या किसी शब्द का कोई अन्य अर्थ निकाल लिया तो—?
तो क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा यही न कि उत्तर न देंगे। इससे ज्यादा तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मन के दूसरे कोने ने संबल प्रदान किया तो उखड़ती सांसों को कुछ राहत मिली।
कई दिनों तक पत्रेत्तर की बड़ी अधीरता रही जो कभी भी व्याकुलता में बदल जाती थी। निगाहें डाकिए की ओर लगी रहतीं। मन नहीं मानता तो स्वयं डाकखाने पहुंच जाती। चिट्ठियां छांट रहे कर्मचारियों से आग्रह करती-‘कोई मेरा पत्र आया हो तो जल्दी दे दीजिए। किसी काम से बाहर जाना था इसलिए खुद चली आई।’
एक दिन तो डाकिए ने झिड़क ही दिया था-‘आप रोज-रोज डाकखाने आकर क्यों परेशान होती हो बहन जी? चिट्ठी आएगी तो घर जाकर दूंगा। सरकार इसी बात की तो तनख्वाह देती है। सिर पर आकर खड़ी हो जाती हो तो छंटाई में दिक्कत होती है।’
अगले ही दिन हाथों में दो पत्र लहराता हुआ, हंसता मुस्कुराता डाकिया दरवाजे पर प्रकट हो गया-‘मुंह मीठा कराओ बहन जी। जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वे खत आ आ गए हैं। लो झटपट खोलो और पढ़ लो। एक नहीं दो-दो खत लाया हूं।’
सचमुच मन खुशी से झूम उठा था। इनमें से एक तो जरूर विद्यालंकार जी का होगा—–क्या पता दोनों ही हो? एक पत्र हो और दूसरी मेरे लिए कोई साहित्यिक रचना।
पर अगले ही पल सारी खुशी गायब——मन में प्रदीप्त हुआ उल्लास का दीप ऐसे बूझ गया जैसे किसी ने ढेर सारा जल उछाल दिया हो। उनमें से एक पत्र तो मेरी समवयस मौसेरी बहन का था। और दूसरे लिफाफे में संपादकीय कार्यालय से वापस लौटी एक अस्वीकृत रचना थी। कभी मेरी मित्रवत अंतरंग जिस मौसेरी बहन के पत्र मुझे आनंद सागर में डुबकियां लगाने को विवश कर देते थे आज उसी का पत्र कड़वी कुनैन की गोली की तरह मुंह का स्वाद कसैला कर गया।——-मैंने दोनों लिफाफों को बिना खोले पढ़े ही किरचा-किरचाकर हवा में उड़ा दिया।
फिर बीतते दिनों के साथ उनके पत्र की प्रतीक्षा स्वयं ही समाप्त होने लगी। साथ ही अधीरता भी चूकने लगी। मन के आशावादी कोने ने दूसरे को दिलासा दे दी-न उत्तर दिया विद्यालंकार जी ने पत्र का तो क्या हुआ? कविताएं लिखना बंद थोड़े ही कर दूंगी। एक न एक दिन कहीं न कहीं छपूंगी भी जरूर। हो सकता है उत्कृष्ट लेखन के लिए कहीं न कहीं पुरस्कार भी मिल जाए। विद्यालंकार जी से ही सब कुछ थोडे़ ही होगा? यह साहित्यकार होते ही दम्भी हैं। जरा सा नाम क्या कमाया कि सब उन्हें अपने सामने बौने लगने लगते हैं। किसी के पत्र के प्रत्युत्तर स्वरूप दो शब्द तक लिखने में अपना अपमान समझते हैं।
मैंने स्वयं ही उनकी ओर से मन पूरी तरह हटा लिया—अब तो भूले से भी यदि उनका पत्र आ गया तो फाड़कर फैंक दूंगी। उनकी छवि को भी अपने हृदय से पूरी तरह मिटा डालूंगी।
परन्तु एक संध्या को कालेज से घर लौटी तो लोहे के मुख्य द्वार के समीप लगी फुलवारी में औंधे मुंह पडे़ एक सफेद रंग के लिफाफे पर निगाह पड़ी। किसका हो सकता है?——संशयात्मक हाथों से उठाया तो कोने में लिखे प्रेषक के नाम को देखकर सहसा विश्वास नहीं हुआ। आंखें मलमल कर बार-बार देखा कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रहीं। अविश्वसनीय था किन्तु था सत्य ही।
पत्र सत्यकाम विद्यालंकार जी का ही था। मेरी तो नस-नस में हर्ष व्याप गया। दिल का कोना-कोना उल्लास से भर उठा। पत्र को मैंने मस्तक से लगा अधरों से चूम लिया। और तत्परता से एक कोना फाड़ पत्र को पढ़ने लगी।
सत्यकाम विद्यालंकार जी के पत्र में लिखा था-प्रियात्मन अपर्णा स्नेहाशीष! तुम्हारा स्नेह के कोहरे से आच्छादित पत्रपुष्प मिला। शब्द व्यंजना देख मन हर्ष के दरिया में डुबकियां लगाने को आतुर हो उठा। दुर्लभ एवं संग्रहणीय पत्र है। तुमने मेरी प्रशंसा में मुझे निःसीम गगन में विचरण करने वाला प्राणी सिद्ध किया है। जबकि मैं तो धरती की धूल को पैरों से स्पर्श करके चलने वाला सामान्य सा क्षुद्र प्राणी हूं। हां कलम का कीड़ा अवश्य हूं। कलम घिसने की निरंतरता बनाए रखना मेरा शौक है। तुमने मेरी साहित्य वारिधि में से बस चुल्लू भर मांगा है। अपने तुम जैसे प्रशंसक को तो मैं पूरा का पूरा सागर दे सकता हूं। आशीष वर्षण के रूप में तुम्हारी कविता का संशोधित रूप भेज रहा हूं। लिखना कविता कैसी लगी? पत्र व्यवहार निर्बाध रूप से जारी रखोगी तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारा शुभाकांक्षी-सत्यकाम विद्यालंकार।
शब्द क्या थे सच्चे मोती थे। सूर्याभा विस्तीर्ण करने वाले मोती—अपनी चमक से नेत्रें को चुंधिया देने वाले मोती निगाह स्थिर नहीं हो पा रही थी। आदि से अंत तक बार-बार फिसली जा रही थी। पता नहीं कितनी बार मैंने उस पत्र को पढ़ा होगा। जैसे उस पर उनकी बार-बार रंग बदलती छवि तैर रही हो।
साथ में एक कविता भी थी। आराधिका शीर्षक से बड़ी सुंदर और उत्कृष्ट कविता थी। नवोदित लेखिका के लिए सुविख्यात साहित्यकार का इससे बड़ा आशीर्वाद और भला क्या हो सकता था? मैं तो कृतज्ञता भार से नत हो गई। प्रफुल्लित इतनी कि भूख प्यास भी गायब और नींद भी आंखों से कोसों दूर। पत्र को हृत्प्रदेश पर रखे नेत्र मूंदे कल्पनाओं के संसार में विचरण करती न जाने कहां से कहां निकल गई।
अगले ही दिन मैंने उनके द्वारा प्रेषित कविता को ‘काव्य सौरभ’ नामक साहित्यिक पत्रिका को प्रेषित कर दिया। और साथ ही आभार व्यक्त करता एक लंबा सा पत्र विद्यालंकार जी को भी लिख दिया। इस बार उन्हें पत्र लिखने में जिस आत्मसंतोष का मुझे एहसास हुआ उसे शब्द जाल में बांधना दुष्कर है। हर्ष एवं उल्लास ने मेरी पीठ पर पंख उगा दिए थे। जिससे मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। मैं आसमान में उड़ने लगी थी।
न जाने मेरे इस दूसरे पत्र में ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या सम्मोहन था कि प्रत्युत्तर स्वरूप उनका पत्र कबूतर की तरह पंख फड़फड़ाता हुआ शीघ्र ही सीधा मेरे हाथों तक आ पहुंचा। ऐसे स्नेेहपगे शब्द, ऐसे मार्मिक भाव, ऐसी अपनत्वभरी भाषा कि मुझे लगा ही नहीं यह किसी अनजान अनदेखे ऐसे व्यक्ति का पत्र है जिससे मेरा कोई नाता नहीं।
पत्रें के इस आवागमन ने कब हम दोनों के मध्य प्रेमांकुर उपजा दिए कुछ भी तो आहट नहीं हो पाई। आभास तब हुआ जब उनके पत्र मुझे अपनी जिंदगी प्रतीत होने लगे। उनका हर पत्र स्नेह का कोहरा बरसाता हुआ आता, रंग बिरंगी तितली की तरह उड़ता हुआ आता, मेरे मन में हर्ष के दीप जलाता हुआ आता। और साथ में होती कोई न कोई कविता। जिसे मैं किसी भी पत्र-पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेजने में विलंब नहीं करती।
और उस दिन तो मेरे हर्ष व उल्लास की कोई सीमा ही नहीं रही जिस दिन ‘काव्य सौरभ’ पत्रिका में मेरी पहली कविता छपी। साथ में मेरा छोटा सा रंगीन फोटो और प्रशंसा के कुछ शब्द भी छपे थे। मोहल्ले में, कालेज में, परिचितों में, सहपाठियों आदि सभी में अपनी कविता दिखाते पढ़ाते मुझे ऐसे गर्व का अनुभव हो रहा था जैसे मैं कितनी बड़ी लेखिका बन गई हूं। चारों ओर शुभकामनाएं व बधाई की बौछार होने लगी। पाठकों के प्रशंसा पत्र भी आने लगे-इतनी अल्प वयस में ऐसी उत्कृष्ट कविता। आश्चर्य भविष्य में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी महान कवयित्री बनोगी।
और महीने भर बाद पुरस्कार का धनादेश हाथों में आया तब तो मैं बल्लियों उछल पड़ी। विद्यालंकार जी ने मेरे उदास जीवन को कैसे रंगबिरंगे फूलों की खुशबू से महका दिया था। इस उपलब्धि का पूर्ण श्रेय उन्हें ही जाता था। अतएव इस पुरस्कार पर भी उन्हीं का अधिकार बनता था। किन्तु उनका यह अधिकार उन्हें सौंपा कैसे जाए? क्या वे प्रत्यक्ष में स्वीकार कर लेंगे? शायद कभी नहीं।
अतएव मैंने उस राशि से पीतल निर्मित नटराज की एक कलात्मक प्रतिमा खरीदकर उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाओं स्वरूप भेज दी। और अनुरोध किया कि मेरे जन्मदिवस पर मेरे सिर पर अपना स्नेहभरा हाथ रख मेरा उत्साहवर्धन करने अवश्य पधारें। उन्होंने प्रेमपगा भरपूर आश्वासन दिया। मैं अधीरता से उनकी प्रतीक्षा करने लगी। बहुत सारी तैयारियां की। घर को ऐसे सजाया जैसे कोई महत्वपूर्ण अतिथि पधार रहा हो। अतिथि की एक झलक पाने को मेरी सहपाठिनें भी सुबह से ही पड़ाव डाले थीं कि क्या पता वह हवा के अल्हड़ झोंके की तरह कब आएं और कब चले जाएं?
उनकी प्रतीक्षा में पल-पल किसी युग जैसा लंबा होता जा रहा था। सुबह से शाम तक पलक पांवड़े बिछाए मैं उनकी राह निहारती रही। किंतु वे नहीं आए। उनके स्थान पर कोरियर से आया एक छोटा सा पत्र जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज न आ पाने के लिए क्षमा! फिर कभी आने का प्रयास करूंगा-सत्यकाम विद्यालंकार।
जैसे किसी ने किसी बच्चे द्वारा मेहनत व लगन से बनाया हुआ रेत का घरौंदा फूंक मारकर उड़ा दिया हो—–वैसे ही उनके न आने से मेरे सपनों का महल कण-कण बिखर गया। आक्रोश में मैंने उनके पत्र को चंदिया चंदिया कर हवा में उड़ा दिया। उनके आतिथ्य के लिए मैंने जितनी भी तैयारियां की थीं सब ध्वस्त कर दीं। और छिलते हुए से शब्द उन्हें लिख भेजें। जन्म दिवस पर न पधारने का धन्यवाद। और अब कभी हमारे घर आना भी मत। मैं तो सोच रही थी कि आपको अपने मन-मंदिर में देवता के रूप में स्थापित कर पूजार्चन करूं। आरती उतारूं। श्रद्धा का भोग लगाऊं और फिर आशीर्वाद प्राप्त करूं। किन्तु आप देवता हैं ही नहीं। देवता होने का ढोंग भरते हैं। आप दम्भी है, छलिया हैं, अभिमानी हैं। आपके हृदय की धरती पर कभी प्रेमांकुर नहीं उपज सकते। आपका दिल पत्थर है तो बस पत्थर ही रहेगा।
मेरा अनुमान था कि मेरे इन विष बुझे शेर जैसे शब्दों का कोई उत्तर नहीं आएगा। और बस संबंध समाप्त। किंतु विद्यालंकार जी के हृदय में अद्भुत धैर्य था। शायद आवेश, आक्रोश, क्रोध, रुष्टता जैसे शब्द तो उनके शब्दकोश में थे ही नहीं। सप्ताह भर बाद ही मधु से भी मधुर, मोम से भी कोमल, पुष्पदल से भी मृदुल शब्द व्यंजना से परिपूर्ण, प्रेमकणों की बौछार सी करता, क्षमा की गंध विस्तीर्ण करता उनका पत्र मेरे हाथ में आया तो मन का सारा मैल, सारी कलुषता पलांश भर में ही धुल गई। किसी आसक्त प्रियतम की हठधर्मी प्रेयसी की तरह मैंने उन्हें इस अनुबंध पर क्षमा किया कि मेरे विवाह समारोह में अवश्य आना होगा। अन्यथा आपकी राह अलग, और मेरी राह अलग। ऐसे मैत्री संबंध भी भला किस काम के जिनमें कभी प्रत्यक्ष भेंट ही न हो सके?
लेकिन पता नहीं उनकी वह कौन सी विवशता थी कि वह वचन देकर भी मेरे विवाह समारोह में उपस्थित नहीं हो सके? मैं बस उनकी राह निहारती रह गई। उन्हें लेकर मैंने न जाने कैसे-कैसे अरमान दिल में संजो रखे थे कि उनके साथ अनेकों फोटों खिंचवाऊंगी, उनमें जो सबसे अच्छा होगा उसे फ्रेम करके अपने ड्राइंगरूम में सजाऊंगी। ताकि आने-जाने वालों को बता सकूं कि ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार से मेरा कितना घनिष्ट संबंध रहा है।
पर मेरे सारे अरमान उस समय किरचा-किरचा होकर बिखर गए जब उनके स्थान पर आया एक छोटा सा पैकेट। जिसमें से निकली एक डायरी, जिसमें प्रणय शीर्षक के अंतर्गत 21 कविताएं उनके हस्तलेख में लिखी थी। क्रोधावेश और उद्विग्नता में थरथराते हाथों से पृष्ठ दर पृष्ठ उलटकर मैंने सरासरा सा दृष्टिपात किया। और एक कोने में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई अनावश्यक, अनचाही हेय वस्तु हो। उन पलों पर ग्लानि होने लगी जिनमें विद्यालंकार जी के अतुलनीय, प्रेक्षणीय व्यक्तित्व व प्रतिभा से सम्मोहित हो मैंने उनकी ओर प्रेमपगी मैत्री का हाथ बढ़ाया था। काश उस समय मैं उनकी स्वार्थपरकता की अंशमात्र भी झलक पा लेती तो कभी मैत्री की डोर से नहीं जुड़ पाती। रोम-रोम घृणा की अग्नि में सुलग उठा-अब उनसे कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं पत्र का उत्तर तक नहीं दूंगी। बाप रे बाप। अपनी प्रसिद्धी पर इतना अभिमान कि अपनी उपलब्धियों के सामने किसी की श्रद्धा, स्नेह व प्रेम का कोई मूल्य नहीं। भाड़ में जाए ऐसे साहित्यकार-दिल के हर कोने से उनकी तस्वीर मिटा डालूंगी और स्मरण तो कभी करूंगी ही नहीं।
ऐसी ही विक्षोभ भरी मानसिकता से लबालब मैं पिया संग ससुराल चली आई।
किन्तु अद्भुत संयोग-रात्रि को जब मुझे मेरे कक्ष में पहुंचाया गया तो पुष्पसज्जित सुहागसेज पर काव्य सौरभ नामक पत्रिका का एक पृष्ठ रखा था। पृष्ठ पर मिलन की रात शीर्षकांतर्गत एक कविता छपी थी। उत्सुकतावश मैंने पढ़ना शुरू किया।
अरे गगन के पंछियों!
तुम मधुर-मधुर से गीत गाना।
है मिलन की रात अनूठी।।
अरे रजनी के स्वामी!
तू चांदनी धरा पर बरसाना।
है मिलन की रात अनूठी।।
अरे विकल प्रणय के क्षणों!
तुम दो दिलों को पास लाना।
है मिलन की रात अनूठी।।
भाषा और शैली चिरपरिचित सी लगी तो दृष्टि शब्दों से फिसलकर कविता के अंत में लिखे नाम पर चली गई। ‘सत्यकाम विद्यालंकार।’ एकाएक वृश्चिक दंश सा लगा—–पलांशभर को चौक सी पड़ी मैं। यहां भी विद्यालंकार? प्रतीत हुआ यह नाम हर जगह हर पल मुझे इसी प्रकार चिढ़ाएगा। भूलना चाहूंगी पर भूल नहीं पाऊंगी। शायद यह नाम मेरा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा।
तभी आंधी तूफान की तरह धड़धड़ाते हुए मेरे सपनों का राजकुमार उस कक्ष में घुसा चला आया। और मुझे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में भरकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला-‘लगता है विद्यालंकार ने यह कविता हम दोनों के मिलन को केन्द्रित कर ही रची है।’
मैं खुशी से उछल पड़ी-‘तो क्या आप भी सत्यकाम विद्यालंकार जी के साहित्य के दीवाने हैं?’
‘भी से क्या तात्पर्य है तुम्हारा?’ अकस्मात उसके चेहरे पर कठोरता उभर आई-‘क्या तुम पहले से ही उसकी दीवानी हो?’
‘जी——ई ई? मेरा मुंह संशय भरे विस्मय से खुला रह गया। समझ नहीं पाई कि उसके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? कहीं पलार्धभर का यह उतावलापन मेरे सपनों की रंगीन दुनिया में रेगिस्तान जैसा शुष्क बंजर ही न उपजा दे?
‘तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि न तो मुझे लेशमात्र भी साहित्य से प्रेम है और न ही इस आशिक मिजाज कवि से मेरा कोई लगाव है।’ अशिष्टता के साथ-साथ उसके स्वर में आवेश का पुट भी झलकने लगा था-‘क्या इसकी कविता पढ़कर तुम्हें नहीं लगा कि यह कितना रसिक होगा?’ उसने मेरे चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया और कहने लगा-‘और तुम यह सुनकर चौंक पड़ोगी कि मैं इस आदमी को भलीभांति जानता हूं। मैंने शोध इसी के सात्रिध्य में किया है। आदमी तो काबिल है बड़ी अच्छी-अच्छी कविताएं लिखता है। बड़े-बड़े कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ कर प्रशंसा पाता है। पर आशिक मिजाज है। पता नहीं किन-किन लड़कियों से पत्र व्यवहार बनाए रखता है। मिलने भी जाता ही रहता होगा? एक बार तो मेरे सामने ही एक लड़की का प्रेमपत्र आया था उसके पास। प्रेषक के रूप में नाम लिखा था-अपर्णा दत्ता।’
पलांशभर को रुक कौंधती उफनती सी दृष्टि से मुझे पस्त करते हुए वह पूछने लगा-‘कहीं वह तुम्हारा ही तो पत्र नहीं था।?’
मैं ऐसे कंपकंपा उठी जैसे भयंकर आंधी में तृण कंपकंपाता है। दिल धाड़-धाड़ उछलने लगा। बड़ी मुश्किल से संयत हो पाई मैं। थूक निगलते हुए बस इतना कह सकी-‘यह क्या कह रहे हैं आप? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। वह कोई और अपर्णा होगी।’
उफ्रफ! कितने उमस भरे थे ससुराल के प्रथम प्रवास के वे दिन। हर पल में उत्तेजना और तनाव समाहित। मेरी खुशियों की नाव मझधार में डूबते-डूबते बची थी। इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ा था। हर शब्द विवेक और संतुलन की तुला पर तोलकर बाहर निकालना पड़ा था। वरना तो हल्की सी भी चूक मेरे जीवन के उमंग और उल्लास भरे हरे-भरे बसंत को वीराने पतझड़ में बदल सकती थी। मेरी खुशियों को अग्निसात कर सकती थी। फिर उसमें भूले से भी कोई फूल नहीं खिल सकता था।
ससुराल से मायके लौटी तो सबसे पहला कार्य मैंने विद्यालंकार जी के स्मृति चिह्नों को मिटाने का किया। ढेर सारे पत्र थे उनके मेरे पास। चुन-चुनकर जलाया। प्रणय नामक डायरी पर निगाह पड़ी तो हाथ उसे भी नष्ट करने की क्रियाशील हो उठे।
किन्तु मेरे साहित्य प्रेमी मन ने विद्रोह कर दिया-विद्यालंकार जी ने कितना परिश्रम किया होगा। कविताओं के इस संसार को रचने में। इस तरह नष्ट करना क्या साहित्य का अपमान नहीं? उनकी स्नेहमयी मैत्री का यह प्रतिदान क्या उचित रहेगा? उनके स्मृति स्वरूप उपहार को अपनी कुंठा की भेंट चढ़ाकर क्या मुझे शांति मिल सकेगी?’
यकायक उस काव्य संग्रह को समाप्त करने को उठे हाथ ठिठक गए। और मन ही मन मैंने एक निर्णय ले डाला—-एक ऐसा वज्र निर्णय जिससे मेरे दांपत्य जीवन में दरार भी पड़ सकती थी। मेरे शांत जीवन में भूकंप भी आ सकता था। मेरा अटल निर्णय था-विद्यालंकार जी के काव्य संग्रह को मिटने न देना, किसी न किसी रूप में उनके अस्तित्व को जीवंत बनाए रखना।
‘प्रणय’ जो अपने छोटे से उर में 21 मधुर संश्लिष्ट व्यंजनायुक्त कविताएं संजोए थी को मैंने अपना और विद्यालंकार जी का संयुक्त नाम अर्थात अपर्णा विद्यालंकार नाम दिया तथा प्रकाशित करा कर बाजार में उतार दिया।
काव्य संग्रह ‘प्रणय’ का बाजार में उतरना था कि चारों ओर धूम मच गई। ‘प्रणय’ में संग्रहीत कविताएं युवा हृदयों की पहली पसंद बन गई। प्रेम की डगर पर कदम बढ़ा रहे हर युवक युवती के हाथ में प्रणय दिखाई देने लगा। मेरे पास प्रशंसा पत्रें का अंबार लग गया। अपने और मेरे निश्छल प्रेम का यह कैसा अनुपम उपहार प्रदान कर दिया था सत्यकाम विद्यालंकार जी ने। किन्तु परिस्थितियों की यह कैसी विडंबना थी कि मैं आभार तक व्यक्त नहीं कर सकती थी उनका। उन्हें आभास तक नहीं करा सकती थी कि उनके इस अमूल्य प्रेमोपहार ने मेरे जीवन में कैसा उजाला कर दिया है। दांपत्य जीवन की बंदिशें इस उजाले की चमक को सत्यकाम जी तक पहुंचाने में मैं स्वयं को लाचार पा रही थी। दो शब्द तक उन्हें नहीं लिख सकती थी। उनके पावन चरणों में श्रद्धा का शीश तक नहीं झुका सकती थी। व्यथा भार से हृदय स्वतः ही दबने झुकने लगा था। मेरी स्वयं की कृतज्ञता किसी विषाक्त शर की भांति हृत्प्रदेश में चुभकर तिल-तिल गलाने लगी थी।
‘चाय चायेÕया! गरमागरम समोसेÕया! सब्जी पूड़ीप्या!—’ तालबद्ध गाड़ी के चलने के स्थान पर सहसा कानों में विचित्र प्रकार के स्वर पड़े तो अतीत के विभिन्न पड़ावों पर ठहरती दौड़ती स्मृतियों की रेलगाड़ी रूक गई।
ट्टषिकेश आ गया था। स्टेशन के बाहर से मैंने तांगा लिया और चल पड़ी अपने परित्यक्त मित्र के अस्थाई आशियाने की ओर।
परमार्थ निकेतन पहुंच पैर सहसा ही अवश हो गए। सत्यकाम जी को पहचानूंगी कैसे? निरंतर प्रवाहमान महाकाल रथ चक्र ने उन्हें कितना बदल दिया होगा। विपन्न स्मृति ने 25 वर्षो पूर्व देखे उस युवा आकर्षक सौंदर्य को क्या आज तक संजो रखा होगा? कोई छायाचित्र भी पास नहीं था, न ही उन्होंने अपनी कभी कोई पहचान लिखी थी।
एक कक्ष के बाहर भारी भीड़ एकत्रित देख मैं उसी ओर बढ़ गई। तरह-तरह की चर्चाएं उभर रही थी। एक सज्जन माथे पर हाथ रख स्वयं ही बुदबुदा रहे थे-‘भगवान ऐसी तिरस्कृत मौत भी किसी को न दे। न जाने कौन अभागा मुसाफिर है जिसे मरने के लिए घर की दहलीज भी नसीब न हो सकी? परिवारजनों का भी कुछ अता पता तक नहीं, जिन्हें कोई सूचना ही दी जा सकती? कम से कम अंतिम संस्कार तो परिजनों के हाथों हो पाता।’
मुझे देख कई लोग मेरी ओर लपक लिए-‘क्या आप ही इस बदनसीब आदमी की रिश्तेदार हैं जो कभी अपना नाम सतकाम तो कभी विद्यालंकार बताता है? कई दिन से अंतिम घडि़यां गिन रहा है, मौत शनैः-शनैः करीब आती जा रही है। पर एक ही रट लगाए है कि जब तक अपरना नहीं आ जाती तब तक नहीं मरूंगा। जल्दी से मिल लीजिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि आपसे अपने दिल की बात कहे बिना ही बेचारा इस संसार से चला जाए?
एक पल को मन मेें आया कि कह दूं यह मुसाफिर मेरा कुछ नहीं लगता। मैं तो भीड़ देख वैसे ही चली आई थी, किसी ने पूछ लिया कि आप इसकी क्या लगती हैं तो क्या उत्तर दूंगी? बात फैलने में देर कितनी लगती है? उड़कर ससुराल तक भी पहुंच सकती है और फिर शक्की पति को पता चलने भर की देर है कोहराम मचा कर रहेगा।
पर भीरु चित्त को मैंने स्वयं ही दिलासा दे दी कि कह दूंगी मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं।
अंधमुंदे कपाटों को खोल भीतर घुसी तो भव्य अतुल्य व्यक्तित्व की ऐसी वीभत्स परिणति देख कलेजा मुंह को आ गया। आंखों से आंसू उमड़ पड़े। एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि 25 वर्षो पूर्व जिस सौंदर्यपुंज को अपने महाविद्यालय में देखा था क्या यह उसी की प्रतिच्छाया है? किन्तु निश्चेतन सूखी काष्ठ जैसे लंबे हाथों में दबी कभी मेरे द्वारा भेंट की गई नटराज की पीतल की प्रतिमा देख संदेह की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई थी कि मैली चीकट चादर बिछे तख्त पर ढहा पड़ा स्मारक स्तंभ मेरी प्रेमपगी मैत्री का ही है।
जैसे किसी ने अस्थि कंकाल पर पतली पीली चादर लपेट दी हो, देह पर मांस की हल्की सी भी परत नहीं रह गई थी। निचुड़े नींबू जैसा पीताभ चेहरा, गड्डे में धंसी चेतनाशून्य आंखें, कपोलों की उभरी हुई हड्डियां, सूखे पपड़ाएं होंठ, रक्तविहीन पांडु ललाट——–नटराज की प्रतिमा को कलेजे से चिपकाए वे गहरी नींद में सो रहे थे या अंतिम अनंत यात्र पर निकल पड़े थे। अनुमान लगाना मुश्किल था। नब्ज टटोलने के लिए मैंने उनका हाथ छुआ तो निर्जीव सी आंखों में कुछ स्पंदन सा हुआ। अस्फुट सा स्वर भी निकला-‘कौन? क्या अपरना आ गई?’
‘जी मैं आ गई हूं।’ मैंने उनके कान के पास मुंह ले जाकर जोर से कहा-‘आंखें खोलकर देखिए सत्यकाम जी! मैं अपर्णा दत्ता आप को अपने साथ ले जाने आई हूं। अब आपको कुछ नहीं होगा।’
निष्प्रभ आंखें खुली और इधर-उधर घूमती हुई मेरे चेहरे पर आकर स्थिर हो गई। और पपड़ाए स्याह होंठ पुनः खुले-‘तो तुम हो अपरना? सचमुच तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारे पत्र बांचकर मैंने जितनी सुंदरता का अनुमान लगाया था उससे बहुत ज्यादा सुंदर, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी।’ इतने से शब्दों में ही वे हांफने लगे तो उन्होंने आंखें मूंद लीं। अंगुली के संकेत से उन्होंने पानी मांगा तो मैंने पास के स्टूल पर रखा गिलास उनके शुष्क होठों से लगा दिया। दो घूंट जल कंठ में उतारने के बाद कुछ सहज हुए तो पूछा उन्होंने-‘पर अपरना तुमने इतनी देर क्यों कर दी यहां आने में? बड़ी मुश्किल से रोके हुए हूं इन्हें। हर पल ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि बस मुझे अपरना के आने तक जिंदा रखना, फिर चाहे अगले ही पल मेरे प्राण खींच लेना।’
दो पल के लिए वे मौन हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने अपनी सूखी लकड़ी जैसी भुजाएं मेरी और बढ़ाई तो मैंने इन्हें पकड़कर बैठा दिया। जीभ फिराकर सूखे होठों को तर करते हुए बोले-‘जानती हो अपरना! मेरे फेफड़े पूरी तरह गल चुके हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। यमराज के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहता हूं। मुझे वचन दो कि पूर्ण मनोयोग से करोगी।’
मैंने उनके कंपकंपाते हाथ अपने हाथों में थाम लिए-‘विद्यालंकार जी मेरे जीवन का बिन्दु बिन्दु आपके उपकारों की भीमशिला के तले दबा पड़ा है। साहित्यिक क्षेत्र में आज मुझे जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त है वह सब आप के कारण। यदि आपका स्नेह व आत्मीयता भरा आश्रय मुझे न मिला होता तो साहित्य विधा के क्षेत्र में कोई मुझे जान भी नहीं पाता। और एक उभरती हुई प्रतिभा खिलने से पूर्व ही मुरझा जाती। आपके उन उपकारों का बदला मैं आपके मात्र एक कार्य से नहीं अपितु अनेकों कार्यो से भी नहीं चुका सकती। आप मुंह से निकाल कर तो देखिए। आपका हर शब्द मेरे लिए आदेश है।’
मेरे हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर उन्होंने तकिए के नीचे से कोई वस्तु निकाली तो मैं अपरिसीम विस्मय से भर उठी। वह मेरेे काव्यसंग्रह ‘प्रणय’ की ही प्रतिलिपि थी। मुझे दिखाते हुए बोले-‘मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारे इस काव्य संग्रह ने बहुत प्रतिष्ठा दिलाई है। बहुत-बहुत बधाई और शत-शत शुभकामनाएं भी। मैं चाहता हूं तुम इस क्षेत्र में बहुत उन्नति करो।’
आत्मग्लानि की ज्वाला से सुलगती मैं लज्जावनत हो दोहरी हो गई-विद्यालंकार जी भलीभांति जानते थे कि ‘प्रणय’ की सारी कविताएं उन्हीं की थी। मैंने उन्हें अपना नाम देने का अपराध किया था। तब भी वह मुझे बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। धन्य था उनका व्यक्तित्व—–धन्य थी उनकी उदारता। कभी उनकी इसी उदारता पर ही तो मर मिटी थी मैं।
निमेष भर रुककर उन्होंने पूछा-‘जानती हो अपरना। मैंने तुम्हें बधाई पत्र क्यों नहीं लिखा? और मैं तुम्हारे विवाह समारोह में भी नहीं आ पाया था? तुमने मुझे अपने जन्मदिवस पर भी बुलाया था तब भी मैं असमर्थ रहा था।
विलक्षण मेधाधनी उस विराट व्यक्तित्व को मैं अपलक, अवाक् निहारती रह गई-क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के इतने सन्निकट होकर भी अपने मस्तिष्क में वर्षो पूर्व की स्मृतियों को ऐसे जीवित रख सकता है जैसे कल की ही बात हो? वे स्वयं ही टूटते बिखरते से स्वर में बताने लगे-‘तुम्हारे आग्रह को तिरस्कृत करने का अपराधी हूं मैं। चाहे जो सजा दे सकती हो। पर अभिलाषा होते हुए भी मैं तुमसे नहीं मिल पाया, मजबूरियां रहीं। जन्मदिवस पर तुम्हारे पास आने का पूर्ण कार्यक्रम सुनियोजित कर लिया था मैंने। पर मेरी पत्नी पैरों में बेडि़यां बनकर अड़ गई-‘मुझे पता है तुम इन कविता कहानियों की आड़ में भोली-भाली लड़कियों से प्रेम संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हो। लेकिन अपने जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।’
मैंने उसे बहुत समझाया बहुत मान-मनुहार की। पर कहते हैं नारी के हृदय में यदि शक का कृमि एक बार कुलबुलाने लगे तो फिर उसे साक्षात इन्द्र भी नहीं मिटा सकते। उसकी जिद के आगे मैं परास्त हो गया था।’ कहते-कहते वे हांफने लगे तो मैंने उन्हें पुनः एक घूंट जल पिलाकर उनकी शुष्कता दूर की।
आसन बदलकर वे पुनः प्रारंभ हो गए-‘तुम्हारे विवाह में मैं आता जरूर, चाहे पत्नी से झूठ बोलना पड़ता। ‘प्रणय’ शीर्षकांतर्गत 21 कविताएं तुम्हें विवाह उपलक्ष्य में प्रत्यक्ष रूप से भेंट करने के लिए ही मैंने तैयार की थीं। किन्तु जब विवाह का निमंत्रण पत्र मिला तो उस अनुपम संयोग पर मैं दंग रह गया तुम्हारे वर के रूप में जो नाम लिखा था वह मेरे एक ऐसे शोधार्थी का निकला जिसने मुझे सदैव चारित्रिक रूप से गलत समझा। हमेशा मेरी शृंगार रस युक्त कविताओं को नई-नई युवतियों को प्रेम जाल में कैद करने का एक अस्त्र समझा। अब तुम्हीं बताओ अपरना। क्या तुम्हारे विवाह समारोह में मेरे उपस्थित रहने से तुम्हारी जिंदगी में जहर नहीं घुल जाता? जो मुझे कभी स्वीकार्य नहीं था। इसीलिए मैंने तुमसे संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया। न तुम्हें बधाई संदेश भेजा, न कोई अन्य पत्र लिखा, न ही मिलने की चेष्टा की।’
सहसा उन्हें खांसी का आवेग उठने लगा जो शनैः-शनैः बढ़ता चला गया। श्वास बहुत तेजी से फूलने लगी और एक झटके के साथ ढेर सारा लाल चमकीला रक्त मुंह से बाहर निकल आया। मैंने उनकी पीठ को अपने हाथों का सहारा न दिया होता तो वह गिर ही पड़ते। मैंने उन्हें धीरे से लिटा दिया तो उन्होंने आंखें मूंद लीं। और संज्ञाशून्य होते चले गए।
मुझे लगा कि पंछी नीलगगन की उन्मुक्त यात्र पर निकल चुका है। उद्विग्न और शोकाकुल मेरे नेत्रें से गरम आंसू निकलकर उनके अस्थिकंकाल जैसे वक्ष को भिगोने लगे।
स्वयं को दिलासा दे मैंने उस कमरे को बाहर से पानी लाकर स्वच्छ किया। उनका चेहरा भी रक्त से सन गया था। उस पर भी पानी के छींटे डाल अपने हाथों से रगड़-रगड़कर धोया। दो चम्मच जल उनके मुंह में भी डाला।
शायद जल की बूंदों का प्रभाव था। अथवा घर्षण का कि ज्योति बुझी मलीन सी आंखें पुनः खुलीं और होठों से अस्फुट स्वर बाहर निकला-‘अपरना मुझे बैठाओ।’
मैंने उन्हें बैठाया तो उनकी सूखी लकड़ी जैसी पतली भुजा ने तकिए के नीचे से एक मोटी सी डायरी निकालकर मेरे हाथों में थमा दी। और तेजविहीन बुझी हुई सी आंखें मेरी रुदन से सूजी हुई आंखों में डालते हुए बोले-‘वेदना’ शीर्षक के अंतर्गत मेरी आत्मकथा है यह। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आत्मकथा की आड़ में मेरे हृदय की वेदना है। मैंने पूरी जिंदगी को स्वाभिमान पूर्वक जिया है। बस यदि हार मानी है तो अपने ही रक्तबीज से। पत्नी की मौत के बाद मेरे बेटों ने ही मेरा स्वाभिमान आहत कर दिया। अपने बेटों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मैंने अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए। जीवन में जो कुछ अर्जन किया था वह सब उन्हें समर्पित कर दिया। किन्तु जब मुझे उनके सहारे की आवश्यकता पड़ी तो दुत्कार और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। और जिस दिन मेरे कानों में उनके विष बुझे शेर जैसे नुकीले शब्द सनसनाते हुए से घुसे ‘हमारे लिए आपने किया ही क्या है? सारी जिंदगी तो कागज नीले-काले करने में गुजार दी। या फिर युवतियों को प्रेमपत्र लिखने में सारी ऊर्जा व्यय कर दी।’ बस उसी दिन से उन दोनों से नाता तोड़ इस परमार्थ निकेतन से नाता जोड़ लिया। आश्रम के अनजान लोगों ने मुझे बहुत प्रेम प्यार व मान-सम्मान दिया। उनका ट्टण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। इस आत्मकथा के माध्यम से मैं समाज के पिताओं को भी संदेश देना चाहूंगा कि कभी भूलकर भी अपनी संपदा अपनी पूंजी बेटों के नाम मत करना। अपनी वृद्धावस्था के लिए सुरक्षित रखना। अथवा किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम को दान कर देना। इस डायरी में मेरे दोनों बेटों के नाम पते भी लिखे हैं। इसे प्रकाशित कराकर एक-एक प्रति उन्हें भी जरूर भेजना।’
इतनी देर तक बोलते-बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। और कंठ सूखने लगा। जलपात्र की ओर उन्होंने पतली सींक जैसी अंगुली घुमाई तो मैंने जलपात्र उठाकर उनके मुंह से लगा दिया। कंठ कुछ आर्द्र हुआ तो भर्राए से अवरुद्ध से स्वर में बोले-‘मुझे माफ करना अपरना! मैंने तुम्हें इतनी दूर बुलाकर—-’
शब्द पूरे नहीं हो सके उनके। देह शिथिल पड़ गई। चेतनाविहीन होकर वे पीछे की ओर लुढ़क पड़े। नाड़ी पर अंगुलियां रखीं तो लेशमात्र भी स्पंदन नहीं था। हृदय की धड़कनें भी शांत पड़ चुकी थीं।
स्पंदनहीन नाड़ी पकड़े-पकड़े मैंने उनके वक्षस्थल पर सिर रख दिया। और फफक-फफककर रो पड़ी। पलकों के भीतर न जाने कितनी देर से नीर संचित हो रहा था जो तटबंध टूटते ही किसी अनियंत्रित नदी की भांति प्रवाहित हो चला।
आंखों के आंसू सूखे तो मुझे स्थिति का भान हुआ। मैं एक ऐसी मृतदेह से लिपटकर रो रही थी जो मेरा कोई भी नहीं था। जिससे मेरा केवल ऐसी मैत्री का नाता था जिसे मैं किसी के भी सामने उजागर नहीं कर सकती थी। वह तो अच्छा हुआ कि आश्रम के लोग गंगा तट पर होने वाली आरती में भाग लेने गए थे। वरना तो अनेकों तरह के प्रश्न उछल सकते थे। संभव था किसी से कोई परिचय भी निकल आता। मैं किसे क्या जवाब देती? और अनर्गल बातें हवा के पंखों पर बैठ यदि मेरे पति तक पहुंच जाती तो–?
तुरंत ही मैंने विद्यालंकार जी की आत्मकथा समाहित डायरी को अपने बैग में ठूंसा और कपाट खोलकर सतर्क निगाहों से बाहर की ओर झांका। अंधकार का झुरमुटा धरती पर पांव पसारने लगा था। आश्रमवासी अभी तक आरती से लौटे नहीं थे। केवल द्वारप्रहरी मुख्य द्वार पर डटे परस्पर वार्ता में तल्लीन थे। एक बार पुनः मैंने उस अभागी मृत देह को जी भरकर निहार हाथ जोड़ अंतिम नमन किया और चुपके से बाहर निकल गई।
आश्रम से बाहर निकल मैंने तांगा लिया और स्टेशन की ओर बढ़ गई। मैं अब भी शंकाकुल थी कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा? कभी कोई यह ही कहने आ पहुंचे कि उस मृत देह को इस तरह लावारिस छोड़ क्यों भागी जा रही हो? उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करती?